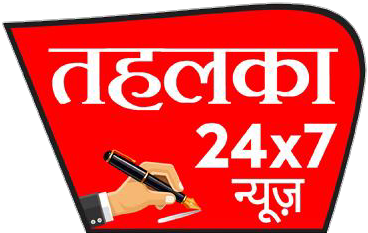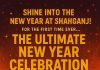बैंकों का विलय समाधान नहीं, बीमारी छुपाता है
# असहायता और लाचारी से जन्मी बेचैनी है यह फैसला, बडा बैंक होगा तो बडा कर्जा लेने-देने में आसानी होगी, भारतीय बैंकिंग का सबसे बड़ा संकट है एनपीए!
कुमार सौवीर
स्वतंत्र पत्रकार
तहलका 24×7
भारतीय बैंकिंग इतिहास में जब भी सरकारें बैंकों को मिलाकर “कम और बड़े संस्थान” बनाने का फैसला लेती हैं, उसका मतलब साफ होता है, कहीं न कहीं ऐसा दबाव बन गया है जिसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करना मुश्किल है। 11 बैंकों को समेटकर तीन बनाने की मौजूदा योजना उसी बेचैनी का परिणाम है। यह कदम जितना सुधार से जुड़ा बताया जा रहा है, उतना ही यह उस भय का संकेत भी देता है कि कहीं अगला बैंकिंग संकट जनता की नजरों के सामने फट न पड़े।

मर्जर की इस हड़बड़ी को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना होगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में तो नहीं, लेकिन उस पर सरकारी हस्तक्षेप की शुरुआत सन-80 से होने लगी थी, जो सन-90 में बडा संकट बन कर सामने आया। दरअसल, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से राजनीतिक निर्देशों पर लोन देना, कॉर्पोरेट को बिना पर्याप्त सुरक्षा के उधार देना और फिर घाटे को वर्षों तक छुपाए रखना एक राजनीतिक स्वाद के तौर पर उमड़ा। 1990 के दशक में जब पहला बड़ा लोन-संकट उभरा था, तब भी यही कहा गया था कि “संविलयन से बैंक मजबूत होंगे।”

लेकिन हुआ उल्टा, बड़े बैंक और बड़े जोखिम लेकर खड़े हो गए। 2000 के बाद जब किंगफिशर, एस्सार, भूषण, एडीएजी और कई अन्य समूहों ने भारी एनपीए झटके, तब भी सरकार ने बैंकिंग में जवाबदेही सुधारने से पहले मर्जर को शॉर्टकट समाधान के रुप में अपनाया।
सबसे बड़ा उदाहरण 2019 का है जब 10 बैंकों को मिलाकर 4 बना दिया गया। उस समय भी दावा यह था कि इन “मेगा-बैंकों” से संचालन सुधरेगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और प्रबंधन दक्ष होगा।

लेकिन तीन साल बाद आरबीआई के आकलनों ने साफ कर दिया कि मर्जर ने सिर्फ यह किया कि खराब लोन को एक बड़े बही-खाते में समेट दिया गया, जिससे घाटा दिखाई कम दिया, जबकि मूल समस्या जस की तस रही। ब्रांचें बंद हुईं, कई जिलों में बैंकिंग कनेक्टिविटी घट गई और स्टाफ पर दबाव इतना बढ़ा कि ग्राहक सेवा की गुणवत्ता तेजी से गिर गई।आज की स्थिति उससे अलग नहीं है, बस चुनौती कहीं ज्यादा गहरी है।कॉर्पोरेट लोन फिर तनाव में हैं।

अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिट कार्ड से लेकर डिजिटल-फिनटेक द्वारा दिए रिटेल कर्ज तक एक अभूतपूर्व स्तर पर हैं और डिफॉल्ट का ट्रेंड अब छिपाया नहीं जा सकता। यह कोई संयोग नहीं कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ऐसी चेतावनी अभी जारी की है। जब तक स्थिति स्थिर लगती रहती है, वैश्विक रेटिंग एजेंसियां चुप रहती हैं। चेतावनी तभी आती है जब बैलेंस शीट की कमजोर दीवारें बाहर से दिखाई देने लगती हैं। अंदरूनी स्रोतों का दावा है कि कई बैंकों की वास्तविक एनपीए की स्थिति आधिकारिक आंकड़ों से बहुत अलग है।

री-स्ट्रक्चरिंग, एवरेजिंग, और खराब लोन को बार-बार ‘गुड’ दिखाने की पुरानी तकनीकें अब काम नहीं आ रहीं। ऐसे में सरकार ने वही आसान तरीका चुना है। बैंकों को जोड़ दो, समस्या बड़ी दिखेगी नहीं और राजनीतिक रुप से सुकून मिलेगा कि “हम सुधार कर रहे हैं।”मौजूदा मर्जर के पीछे राजनीतिक कारण सबसे स्पष्ट हैं। सार्वजनिक बैंक अब बैंकिंग कम और सरकारी नीतियों के औजार ज़्यादा बन गए हैं। चुनावी वर्षों में लोन वितरण का दबाव बढ़ता है। कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों पर अत्यधिक निर्भरता की प्रवृत्ति मजबूत हुई है।

जब किसी कॉर्पोरेट को आधा दर्जन बैंकों से पैसे मिलते हैं, और वह डिफॉल्ट करता है तो नुकसान पूरे बैंकिंग तंत्र में फैल जाता है। पिछले 20 वर्षों में लगभग हर बड़ा कॉर्पोरेट एनपीए, राजनीतिक संरक्षण और नियामकीय ढिलाई की मिलीजुली देन रहा है। इस पृष्ठभूमि में यह मर्जर “साजिश” नहीं तो कम से कम इतना तो है कि इसके जरिए सरकार बैंकिंग सिस्टम की वास्तविक बीमारी को जनता की आंखों से ओझल रखना चाहती है। क्योंकि बीमारी बहुत गहरी है। बोर्ड नियुक्तियों पर राजनीति का नियंत्रण, रेटिंग और वैल्यूएशन में कॉर्पोरेट दबाव, आरबीआई का कमजोर निगरानी ढांचा और सबसे खतरनाक, फिनटेक आधारित अनसिक्योर्ड क्रेडिट का ज्वालामुखी।
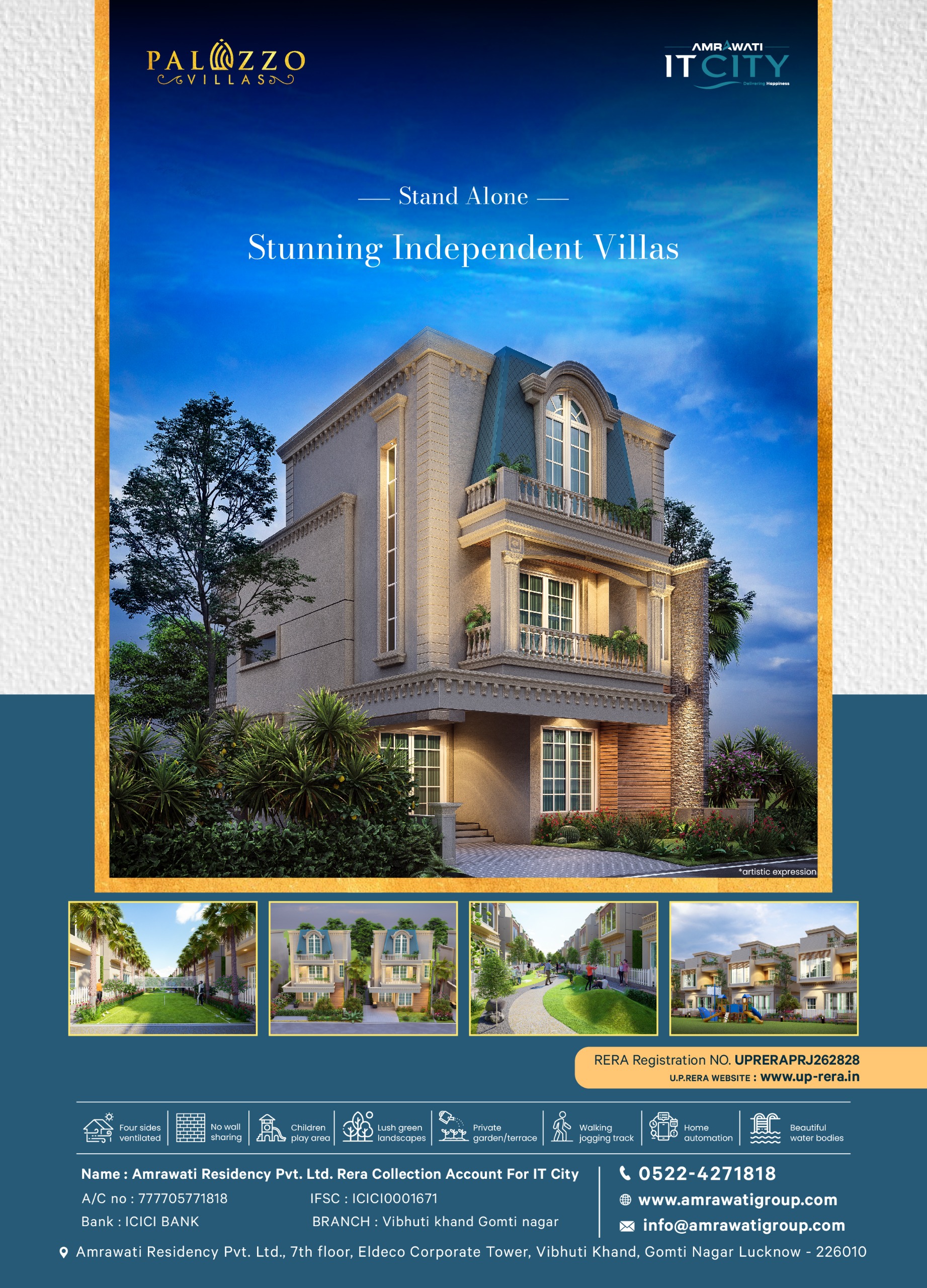
कोविड के बाद बाजार की मांग को बढ़ाने के नाम पर लोगों को ऋण लेने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया गया। ईएमआई आधारित जीवन सामान्य बना दिया गया और बैंकिंग सिस्टम ने इसे “ग्राहक विस्तार” कहा। पर यह विस्तार असल में बम की टिक-टिक थी, जिसके फटने का समय अब निकट लग रहा है। रिटेल क्रेडिट की यह विस्फोटक वृद्धि तब और खतरनाक हो गई जब बैंक खुद फिनटेक कंपनियों पर निर्भर हो गए, जिनकी जोखिम मूल्यांकन प्रणालियां बेहद कमजोर थीं। विदेशी दबाव भी इस कहानी का एक हिस्सा है।
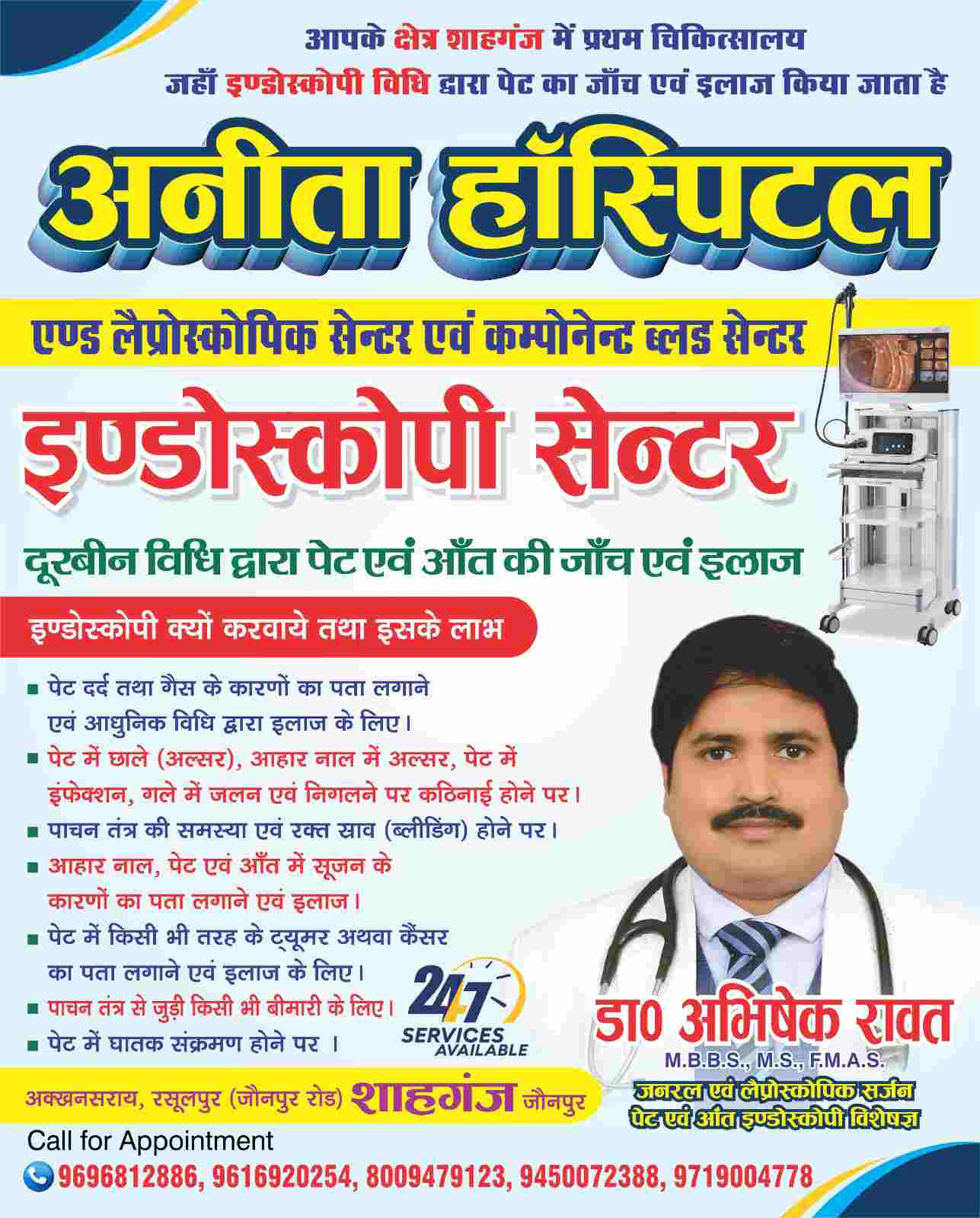
आईएमएफ, एफएटीएफ और रेटिंग एजेंसियां वर्षों से कहती आई हैं कि भारत में पीएसयू बैंकों की संख्या बहुत ज्यादा है। वे चाहते हैं कि वित्तीय तंत्र बड़े ब्लॉकों में सिमट जाए, क्योंकि इससे निगरानी और नियंत्रण आसान हो जाता है। यह मॉडल यूरोप में अपनाया गया था, लेकिन वहां भी 2008 के दौरान यही हुआ कि कुछ मेगा-बैंकों की विफलता ने पूरे महाद्वीप को आर्थिक संकट में धकेल दिया। केंद्रित जोखिम हमेशा सुनामी की तरह होता है।धीरे आता है पर तबाही बहुत बड़ी छोड़ जाता है।

सरकार ने दावा किया है कि पिछले सभी सुधार आईबीसी कानून, बैड बैंक, पूंजी-इन्फ्यूजन, डिजिटल मॉनिटरिंग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वास्तव में काम कर रहे होते, तो मर्जर की इतनी हड़बड़ी क्यों होती? मर्जर कभी भी तब नहीं किए जाते जब चीजें ठीक चल रही हों। मर्जर हमेशा तब होते हैं जब फाइलों में छिपी सच्चाई बाहर आने लगती है।इतिहास यही बताता है कि मर्जर लक्षण छुपाते हैं, बीमारी नहीं। बैंक का आकार बड़ा हो जाता है, पर संस्कृति वही रहती है, अनुशासनहीन राजनीतिक दबाव में झुकी हुई और कॉर्पोरेट बॉरोअर्स के सामने असहाय।

जब वही संस्कृति बड़े बैंक में प्रवेश करती है, तो उसकी विफलता का असर भी कई गुना बढ़ जाता है। इस कदम का सीधा परिणाम यह होगा कि शाखाएं घटेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच कम होगी, और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता गिरेगी। स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और आंतरिक प्रक्रियाएं वर्षों तक गड़बड़ रहेंगी। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि सभी समस्याएं कुछ बड़ी बहीखातों में इकट्ठी हो जाएंगी और अगर आने वाले वर्षों में इनमें से किसी एक बैंक को बड़ा झटका लगा तो पूरा वित्तीय तंत्र उसके साथ डगमगा जाएगा। मर्जर को सुधार कहना सुविधाजनक है, पर यह असल में असुरक्षा की स्वीकारोक्ति है।

यदि सरकार वास्तव में बैंकिंग सुधार चाहती तो उसे गवर्नेंस में पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप की रोक, आरबीआई की स्वतंत्रता और कॉर्पोरेट जवाबदेही की कठोर प्रणाली बनानी होती। लेकिन इन कदमों से सत्ता की सुविधा घटती है, इसलिए आसान रास्ता चुना गया। बैंकों को बड़ी गठरी में बांधो और दिखाओ कि भार कम हो गया है।

भारतीय बैंकिंग इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां यह मर्जर शायद कुछ महीनों के लिए राहत दे दे, लेकिन कुछ वर्षों बाद इसका वही परिणाम होगा जो 2019 के मर्जर का हुआ। समस्याएं और बड़ी, जोखिम और व्यापक। अब जो कुछ हो रहा है, वह सुधार नहीं, तूफान से पहले का शोर है। सत्ता चाहती है कि यह तूफान उसकी बारी तक न पहुंचे, पर बैंकिंग तंत्र में जो गहराई तक सड़ चुका है, वह केवल मर्जर से ठीक नहीं होने वाला।