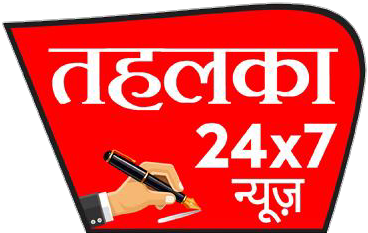47 फीसदी मुकदमे फर्जी साबित, राज्य सरकार जिम्मेदारी ले
# बेबुनियाद मुकदमा से निराश जिन्दगी को लहलहाने की कोशिश, हताश जिन्दगी मुआवजा दिलाने की कोशिश में है जस्टिस विक्रमनाथ, योगी राज में 15 हजार को पुलिस ने सीधे घुटने पर गोली मारी क्यों?
लखनऊ।
कुमार सौवीर
स्वतंत्र पत्रकार
हम घटनाओं पर चर्चा तो करते हैं, पकड़े गए अभियुक्तों पर बढ़-चढ़कर लानत भेजते हैं, लेकिन कानून के तराजू में निर्दोष साबित हुए बेगुनाहों पर बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों की जस्टिस विक्रम नाथ वाली बेंच के ताजा फैसले ने जेल और समाज में दोहरी जेल काट चुके नागरिकों को मुआवजा देने का जो फैसला किया है, वह देश में न्याय जगत में बेमिसाल बन सकता है। हालांकि जस्टिस पीएन भगवती और चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने 1980 के दशक में इस दिशा में सटीक शुरूआत की थी।

रुडुल साह और भीम सिंह जैसे मामलों ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मुआवजे की नींव रखी थी, पर वो नींव कच्ची सड़क तक ही सीमित थी। कुछेक फैसलों में मुआवजा मिला, बाकी में याचिकाएं धूल फांकती रहीं। लेकिन अब जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने और इस मामले पर संसद में कानून बनाने का जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे गलत अभियोजन के शिकार निर्दोषों को मुआवजा मिलने की पक्की सड़क बनने की संभावनाएं बलवती हो रही हैं।

भारत की न्याय व्यवस्था का एक काला सच यह है कि हर साल हजारों लोग फर्जी आरोपों में फंसकर सालों जेल में सड़ते हैं। बरी होने पर उन्हें सिर्फ “न्याय मिला” कहकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन खोया हुआ समय, मानसिक आघात, परिवार का टूटना और सामाजिक कलंक इनकी भरपाई कौन करेगा?सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 से इस सवाल पर संघर्ष किया है और 2025 में जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इसे ऐतिहासिक मोड़ दिया है। यह लेख उन सभी पहलुओं को जोड़ता है।

पुराने सिद्धांत, हालिया फैसले, कानूनी खाई और भविष्य की उम्मीद। लेकिन अब सवाल यह है कि फर्जी मुकदमों के शिकार निर्दोष कैदियों को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? जस्टिस विक्रम नाथ की तीन जजों वाली बेंच से लेकर अन्य बेंचों तक के फैसलों ने इसकी नींव रखी है, फिर भी व्यवस्था में गहरी दरारें बाकी हैं। नींव 1983 में पड़ी जब रुडुल साह ने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। उन्हें 1953 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, 1968 में बरी हुए, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही से 1972 तक जेल में रहे।

जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़, एएन सेन और आरबी मिश्रा की बेंच ने पहली बार सार्वजनिक कानून उपाय के तहत राज्य को 30 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसला 1 अगस्त 1983 को आया और बिहार सरकार ने 5,000 रुपये पहले ही भुगतान कर दिए थे। शेष रुपये दो सप्ताह के अंदर चुकाने का निर्देश था। अदालत ने कहा कि गैरकानूनी हिरासत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए अलग नागरिक मुकदमे की जरुरत नहीं। यह फैसला भारत में पब्लिक लॉ रेमेडी की शुरुआत बना। लेकिन क्या यह लागू हो पाया? आंशिक रुप से हां!

इसने बाद के मामलों में मिसाल कायम की, जैसे 1993 के नीलाबती बेहेरा बनाम ओडिशा में जस्टिस जेएस वर्मा की बेंच ने पुलिस हिरासत में मौत के लिए 1.5 लाख रुपये मुआवजा दिया, उसी सिद्धांत पर। फिर भी पूर्ण रुप से लागू होना दूर की कौड़ी रहा, क्योंकि राज्य की जवाबदेही पर कोई बाध्यकारी कानून नहीं बना। इसके बाद कई मील के पत्थर आए। 1981 में भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर मामले में जस्टिस पीएन भगवती की बेंच ने एक विधायक की गलत गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा दिया।

1997 में डीके बसु दिशानिर्देशों ने गिरफ्तारी के 11 नियम तय किए, जिनके उल्लंघन पर मुआवजा अनिवार्य हो गया। हाल के वर्षों में भी यह सिलसिला जारी रहा। 2025 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक मामले में चार महीने की गलत हिरासत के लिए 5 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। लेकिन 2025 का असली मोड़ जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच लेकर आई। 15 जुलाई को कट्टावेलाई बनाम तमिलनाडु मामले में जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की तीन जजों वाली बेंच ने मौत की सजा पा चुके एक कैदी को गलत जांच के आधार पर बरी किया।
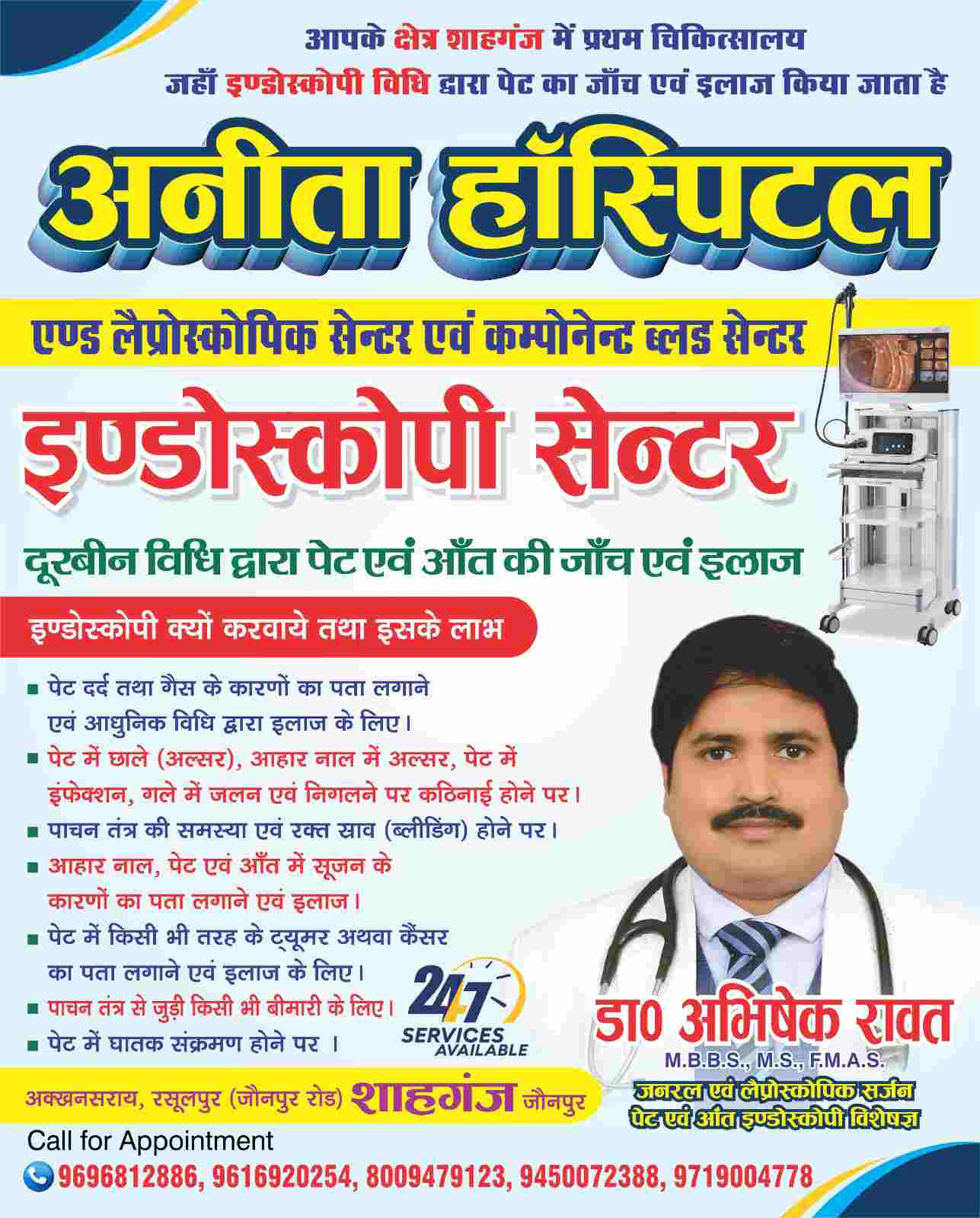
अदालत ने संसद से गलत अभियोजन के लिए कानून बनाने की मांग की, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में ऐसे कानून मौजूद हैं, लेकिन भारत में नहीं। बेंच ने लॉ कमीशन की 277वीं रिपोर्ट का जिक्र किया जो गलत अभियोजन को सीमित न मानते हुए लंबी कैद पर मुआवजे की जरुरत बताती है। फिर 27 अक्टूबर को उसी बेंच जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने एक और मामले में ऐतिहासिक कदम उठाया। याचिकाकर्ता को 2013 में गिरफ्तार किया गया, 2019 में मौत की सजा सुनाई गई और 2025 में बरी कर दिया गया।
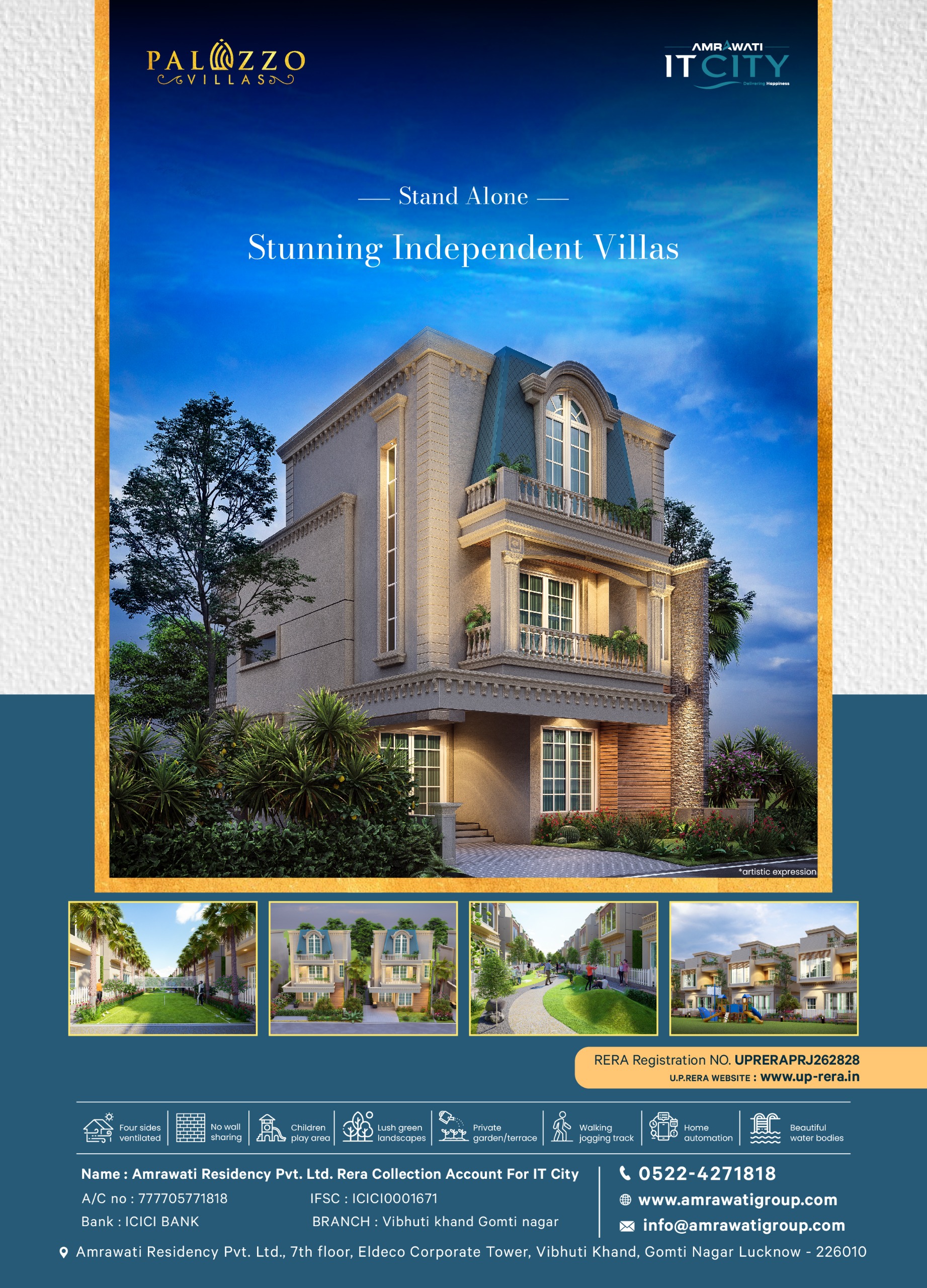
अदालत ने चिंता जताई कि भारत में दोषसिद्धि दर सिर्फ 54 प्रतिशत है, यानी 46 प्रतिशत लोग गलत फंस सकते हैं।यह आंकड़ा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार है, जो लोअर कोर्ट्स और हाईकोर्ट्स के ट्रायल्स पर आधारित है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर। सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में दोषसिद्धि दर ऊंची जो लगभग 70-80 प्रतिशत होती है, लेकिन निचली अदालतों में यह कम है, जो फर्जी मुकदमों की समस्या को उजागर करता है।

बेंच ने महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी और गलत अभियोजन के शिकार पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया। दो अन्य समान याचिकाएं भी जोड़ी गईं। इन फैसलों के बावजूद कानूनी खाई बरकरार है। सीआरपीसी की धारा 357ए पीड़ित मुआवजा योजना तो है, लेकिन यह अपराधी से वसूली पर केंद्रित है, राज्य की जिम्मेदारी पर नहीं। धारा 357ए (1) के तहत राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर योजना बनाती हैं, और अगर अपराधी का पता न चले या ट्रायल न हो तो पीड़ित सीधे राज्य या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मुआवजा मांग सकता है।

लेकिन फर्जी मुकदमों में राज्य ही दोषी होता है, फिर भी मुआवजा राज्य की जेब से जाता है, सार्वजनिक कोष से। पहले यह अपराधी की जिम्मेदारी थी (धारा 357), लेकिन 2008 के संशोधन से राज्य की भूमिका बढ़ी। फिर भी अमल में कमी है।कई राज्य योजनाएं अधर में लटकी हैं और मुआवजा मिलना दुर्लभ। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में Wrongful Conviction Compensation Act है। अमेरिका में 35+ राज्य स्तर पर 1980-90 के दशक से (जैसे कैलिफोर्निया 1987 से, ब्रिटेन में 1988 से क्रिमिनल जस्टिस एक्ट, आर्टिकल 14(6) ICCPR पर आधारित)।

कनाडा में 1990 के दशक से, न्यूजीलैंड में 2001 से गाइडेड डिस्क्रेशनरी सिस्टम और ऑस्ट्रेलिया के ACT में 2004 से, ये कानून निर्दोष को सालाना 50,000-1,00,000 डॉलर तक देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई यूनिफॉर्म कानून नहीं।असल जिंदगियों में यह पीड़ा साफ दिखती है। विष्णु तिवारी 17 साल बाद 2021 में बरी हुए, लेकिन मुआवजा अलग याचिका से मांगना पड़ा। 7/11 बम विस्फोट के 12 आरोपी 19 साल बाद जुलाई 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट से बरी हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। मुआवजा अभी लंबित है। अक्षरधाम मामले में तो 2014 में बरी होने के बावजूद मुआवजा अस्वीकार कर दिया गया, ताकि गलत नजीर न बने।
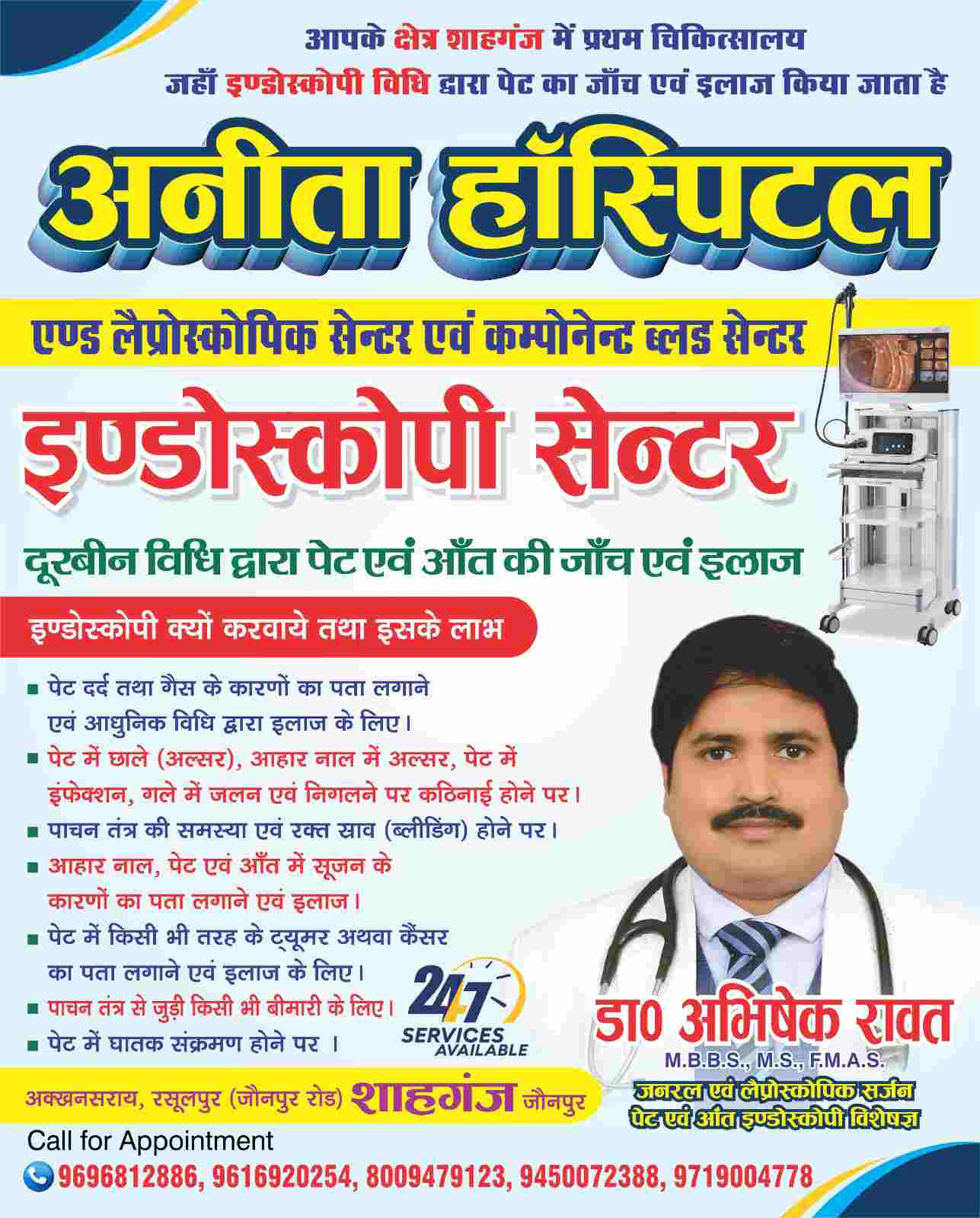
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बरी होने पर मुआवजा देना खतरनाक होगा।भविष्य में उम्मीद है कि 2026 तक अदालत की निगरानी में राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनेंगे। Wrongful Prosecution Bill संसद में प्रस्तावित हो सकता है और सीआरपीसी 357ए का विस्तार राज्य स्तरीय मुआवजा कोष तक हो सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने साफ कहा कि यह सिर्फ कानूनी सवाल नहीं, मानवीय सवाल है। फर्जी मुकदमे में फंसा व्यक्ति दो बार सजा पाता है। पहले जेल की, फिर बरी होने के बाद खाली हाथ लौटने की।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में दरवाजा खोला, 2025 में जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने सड़क बनाने का वादा किया। अब बारी संसद की है, क्या वह कानून बनाएगी, या अगला रुडुल साह फिर 14 साल इंतजार करेगा?लेकिन यह सिर्फ पुरानी कहानी नहीं। योगी सरकार की पुलिस तो एक नया इतिहास बना रही है। कोर्ट के पहले ही अभियुक्त को सीधे घुटने पर गोली मार कर उसे हमेशा के लिए अपाहिज बनाने पर आमादा है। मार्च 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिनमें 256 कथित अपराधी मारे गए, 9,467 घायल हुए।

कई दारोगा ही नहीं, बल्कि कई एसपी, आईजी और एडीजी तक इस तरह के अपराध में लिप्त हैं और उनकी करतूतें अब सिंघम या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर डुग्गी बजा रही है। 2025 में नोएडा और कानपुर में कोर्ट ने 12 पुलिसवालों पर फर्जी एनकाउंटर के चार्जशीट लगाई, सबूत प्लांट करने के आरोप साबित हुए। एनएचआरसी ने भी नोटिस जारी किए, लेकिन सरकार इसे “जीरो टॉलरेंस” बताती है। यह एनकाउंटर राज न्याय के सिद्धांतों, निष्पक्ष ट्रायल, संदेह का लाभ आरोपी का अपमान है। निर्दोषों को मुआवजा देने की बात तो दूर, यहां तो बिना ट्रायल के सजा दी जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों को देखकर बताइए कि न्याय सिद्धांत के पैमाने पर भारत किस पायदान पर है? एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय की बेंचें मुआवजे के दिशानिर्देश बना रही हैं, दूसरी तरफ राज्य स्तर पर फर्जी मुकदमे और एनकाउंटर बेलगाम हैं। दोषसिद्धि दर 54 फीसदी होने से साफ है कि निचली अदालतों में जांच की खामियां आम हैं। अमेरिका-ब्रिटेन जैसे देशों से तुलना करें तो भारत का सिस्टम विकसित है।अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा मजबूत है और PIL जैसे उपकरण हैं।

लेकिन अमल में यह तीसरे विश्व का न्याय है। राज्य की जवाबदेही कमजोर, मुआवजा योजनाएं कागजी, पुलिस का मनमाना रवैया। लॉ कमीशन की सिफारिशें धूल फांक रही हैं। भारत को न्याय के पैमाने पर मध्यम पायदान (ग्लोबल इंडेक्स में 79वां रैंक, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024) से ऊपर चढ़ना होगा।कानून बनाने, पुलिस सुधार और मुआवजा को अनिवार्य बनाने से। वरना, निर्दोषों का इंतजार जारी रहेगा और न्याय सिर्फ किताबों तक सीमित।